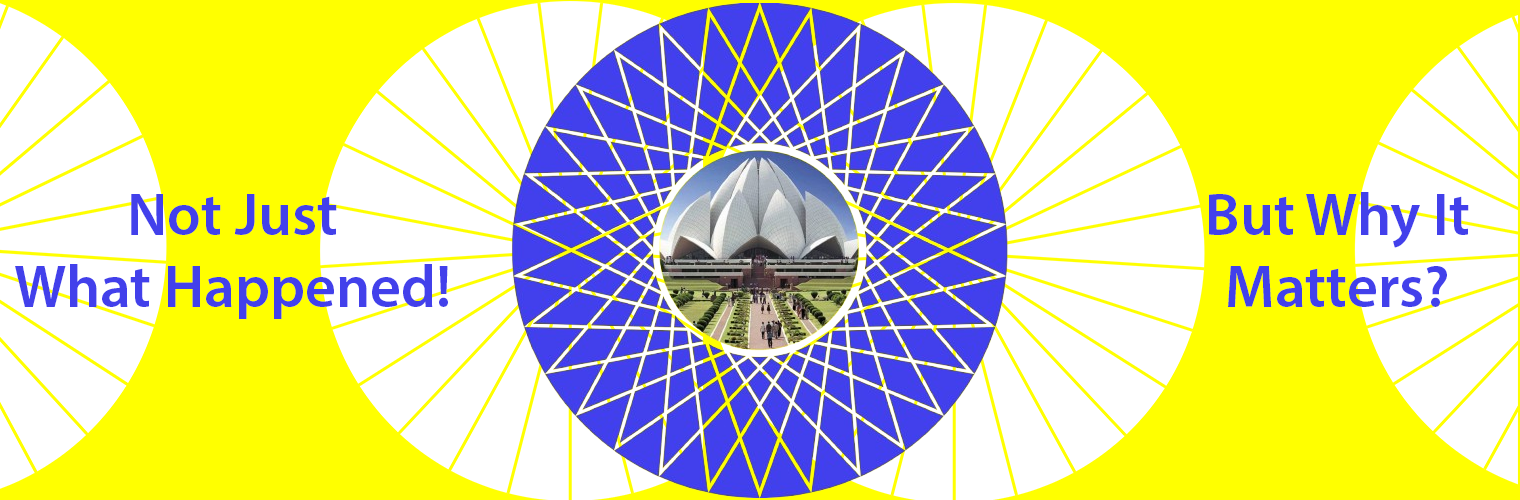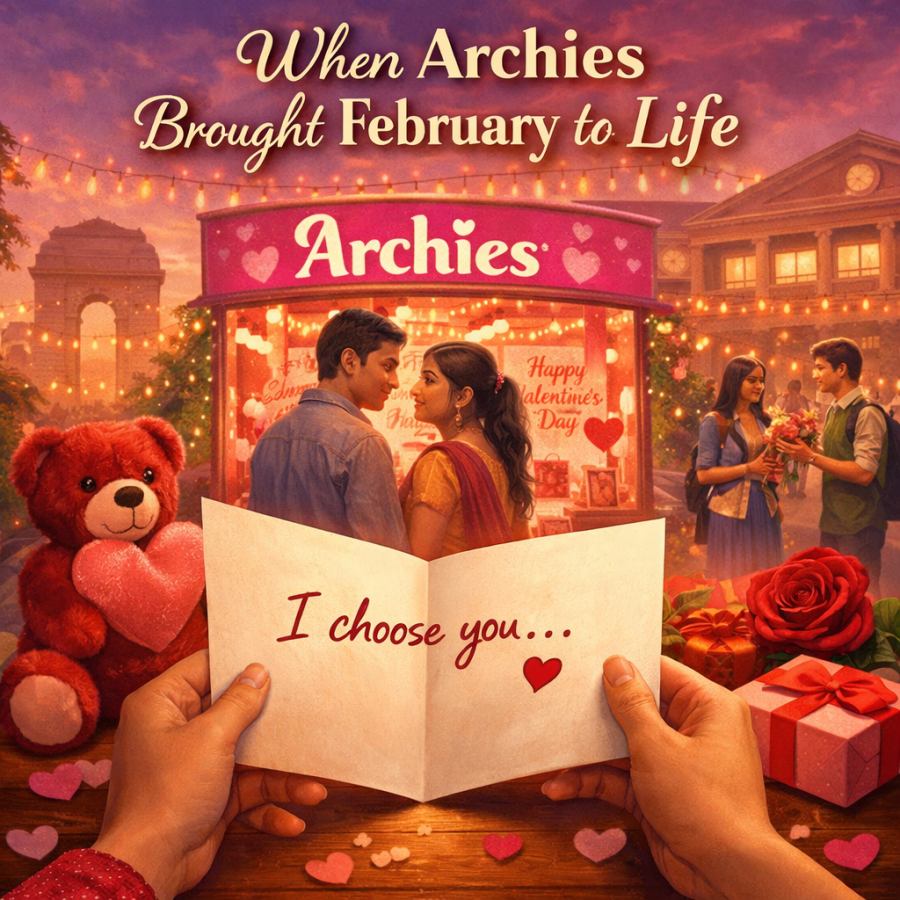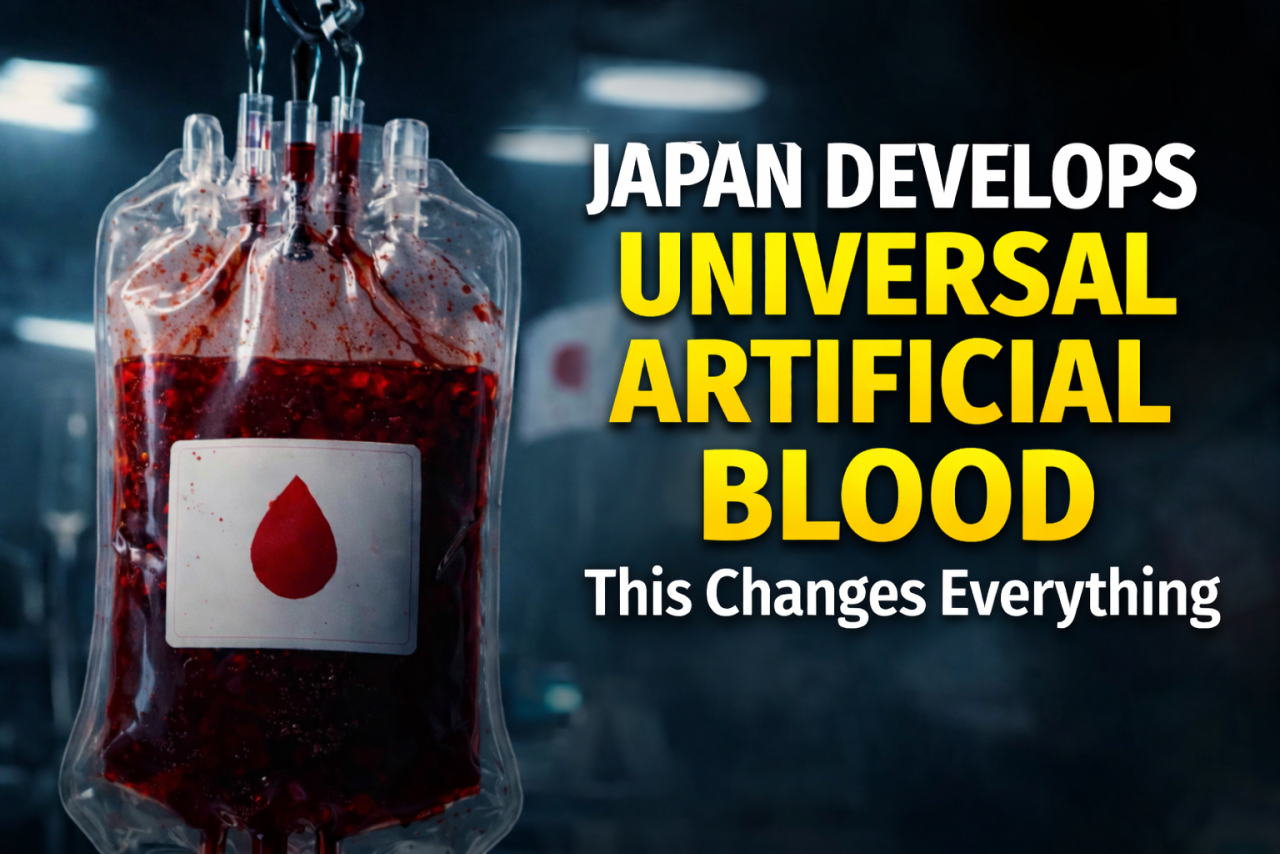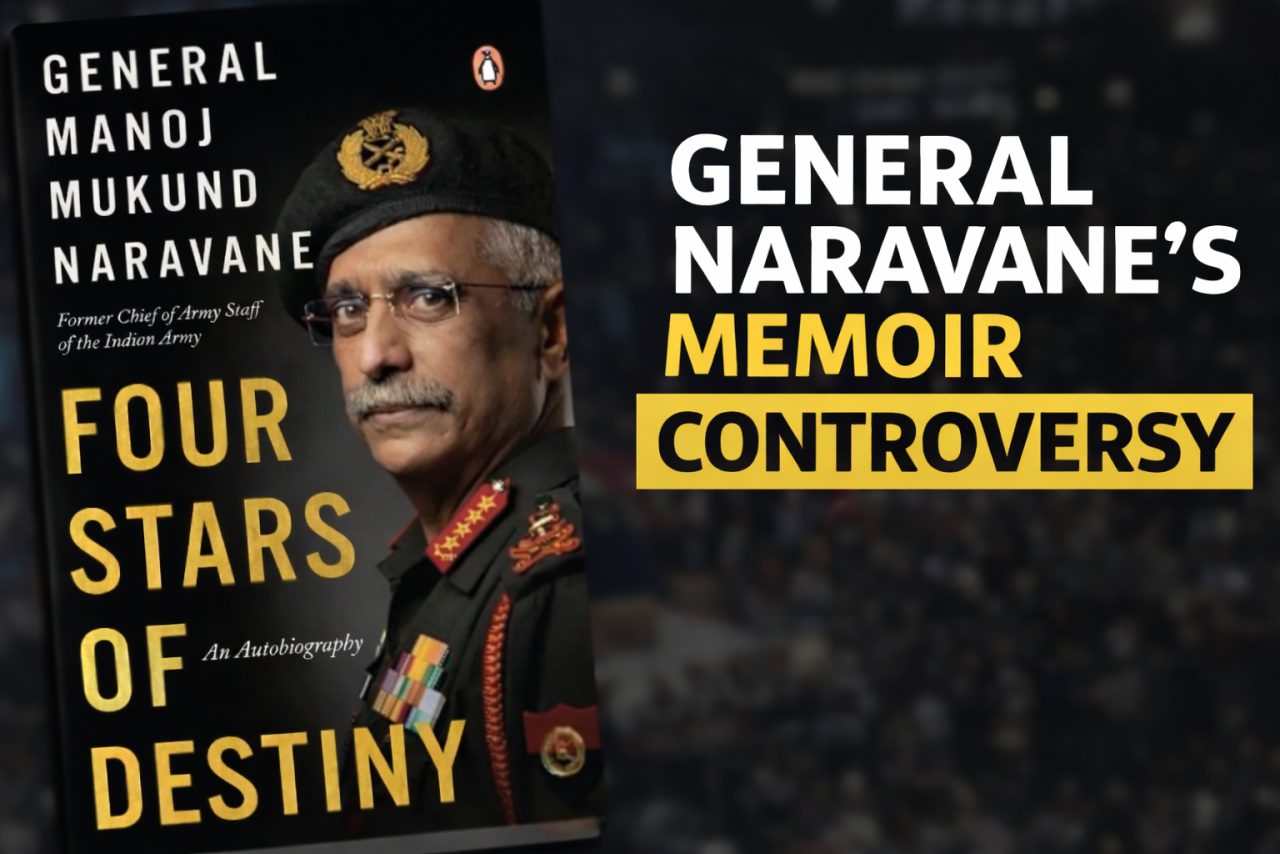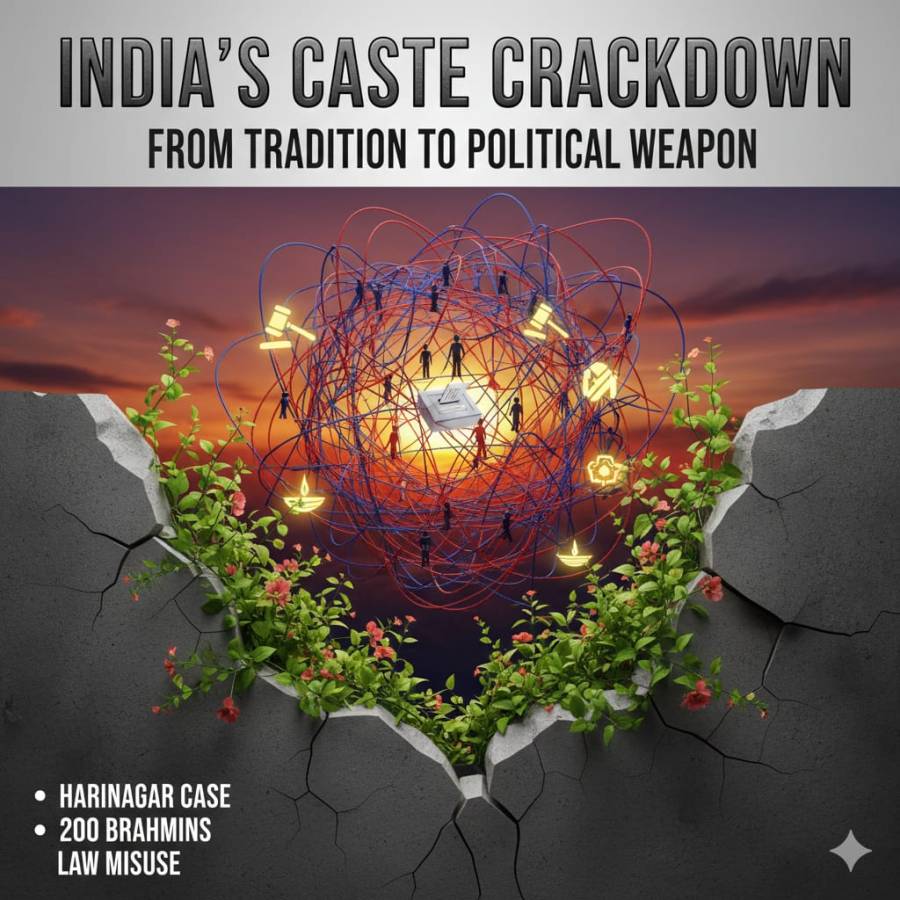बिहार का प्रवासी
मिट्टी अब भी महकती है, पर मन में धुआँ भरा है,
हर घर से कोई निकला है, कोई लौट नहीं रहा है।
पगडंडी पर बचे हैं बस पदचिन्ह पुराने,
जहाँ बचपन खेला करता था, अब झाड़ियों के ठिकाने।
स्कूल की खिड़कियों पर धूल की परतें जमी हैं,
किताबें हर बाढ़ में गलती हैं कहीं।
मास्टर खोया सेंसस में, बच्चे ढो रहे बोझ,
ज्ञान की लौ बुझी, और अंधेरा हुआ रोज़।
गाँव के चौक पर अब सन्नाटा बोलता है,
जहाँ हँसी गूंजती थी, अब डर डोलता है।
दिनदहाड़े मरते हैं सपने, लाशें गिनती भूल गईं,
इंसाफ़ की सुबह जैसे किसी और दिशा में खुल गई।
फैक्ट्री का सपना देखा था, ईंट भी न रखी गई,
धान कटते ही धरती फिर बेरोज़गारी से ढँकी गई।
न उद्योग, न अवसर, बस इंतज़ार की नदी,
जिसके किनारे बैठा है हर नौजवान अभी।
रेल की सीटी अब भी अलविदा कहती है,
हर प्लेटफॉर्म पर एक कहानी बहती है।
माँ की आँखें पथरा जाती हैं चौराहे तकते,
रोज़ बात तो होती है, पर बात नहीं बनती।
शहर में उसे “बिहारी” कहकर पुकारा गया,
जैसे मेहनत उसका अपराध ठहराया गया।
पर वही मज़दूर उठाता है शहरों की दीवारें,
और लौटता है मिट्टी में, अपनी थकान के सहारे।
पीढ़ियाँ गुजर गईं टिकट कटवाते हुए,
एक लौटती है, दूसरी जाती हुए।
यह चक्र कोई जीवन नहीं, एक दर्द का गीत है,
जहाँ सपनों की कीमत बस पेट की रीत है।
बिहार, तेरे गाँव अब भी उजाले की आस में हैं,
जहाँ बच्चे अब भी “मास्टर बनब” के विश्वास में हैं।
पर रोटी से पहले किताब कब आएगी यहाँ,
यह सवाल गूँजता है हर बुझती चिराग में वहाँ।
फिर भी तेरी मिट्टी में कुछ तो अडिग है,
आस्था, श्रम और उम्मीद का अद्भुत संगीत है।
हर प्रवासी के मन में तेरी ही तस्वीर है,
हर लौटते कदम में — तेरी ही तक़दीर है।
-गौतम झा