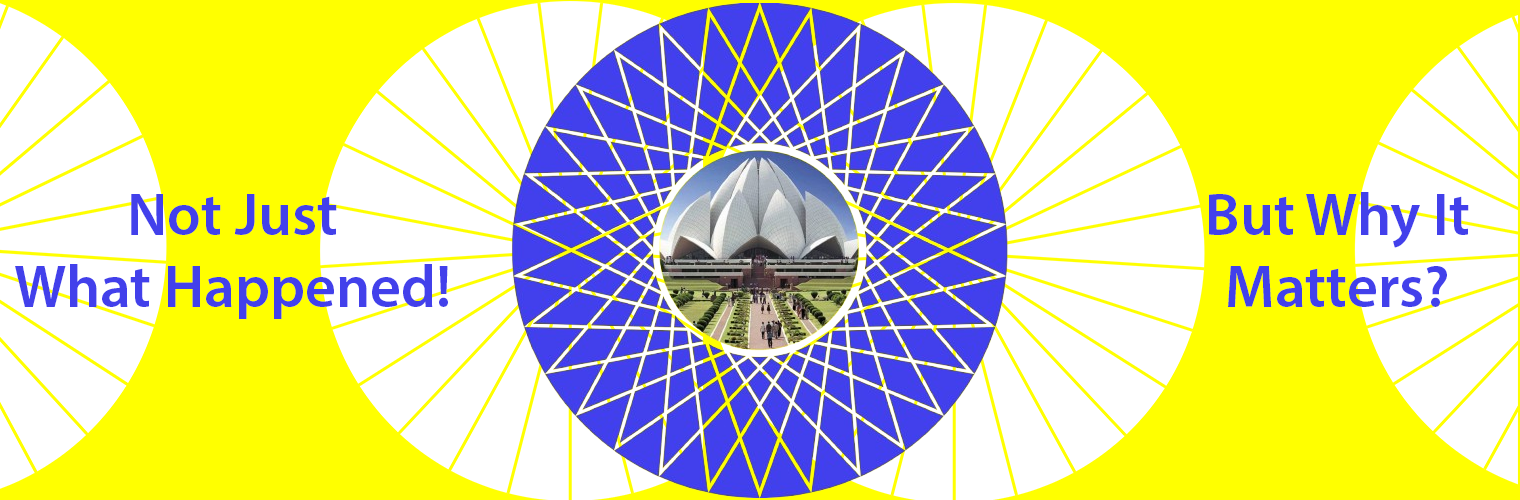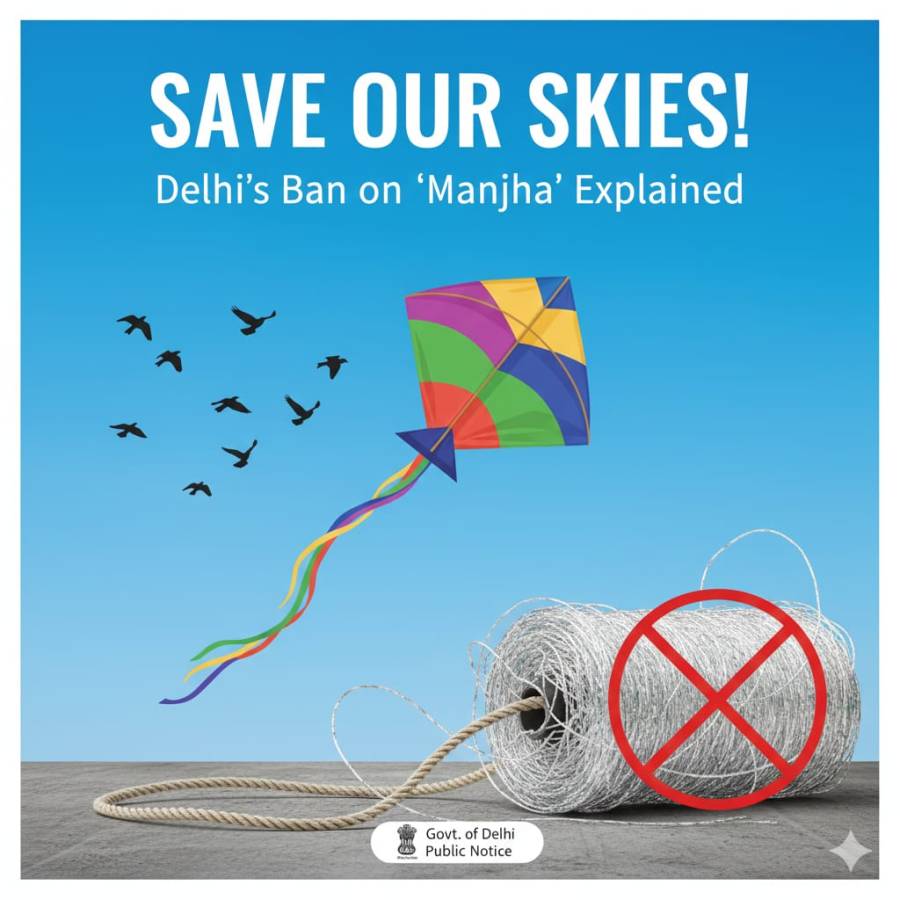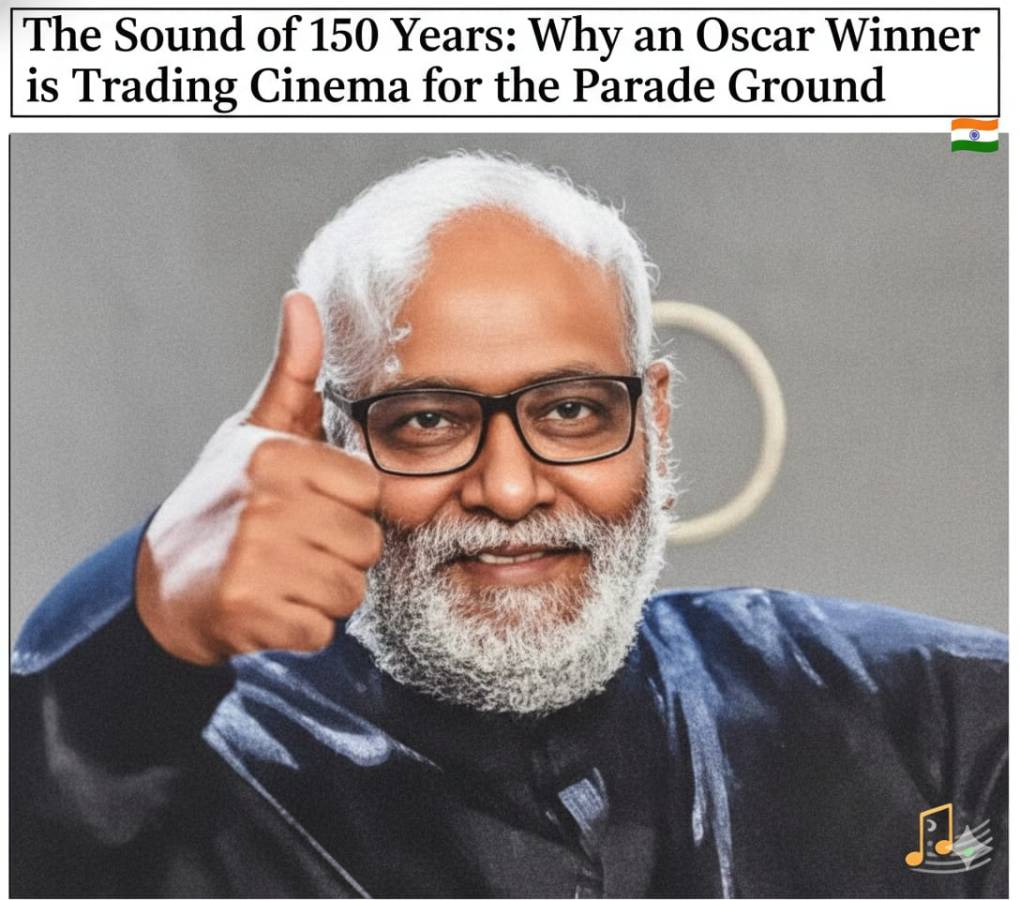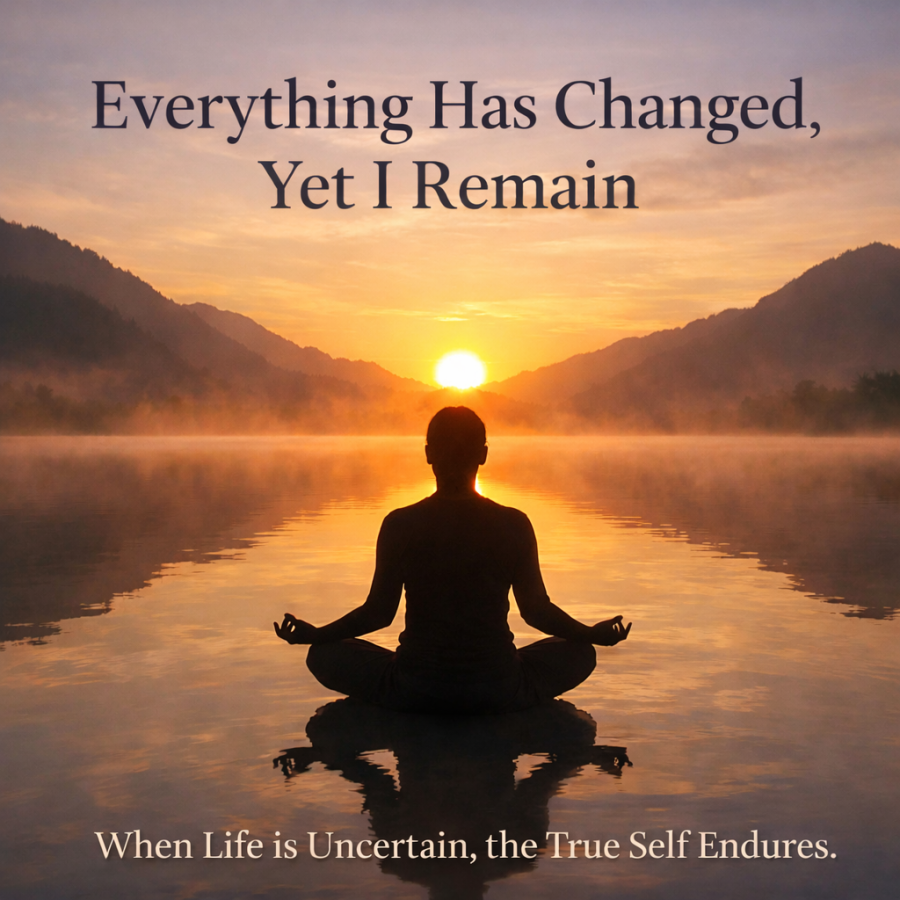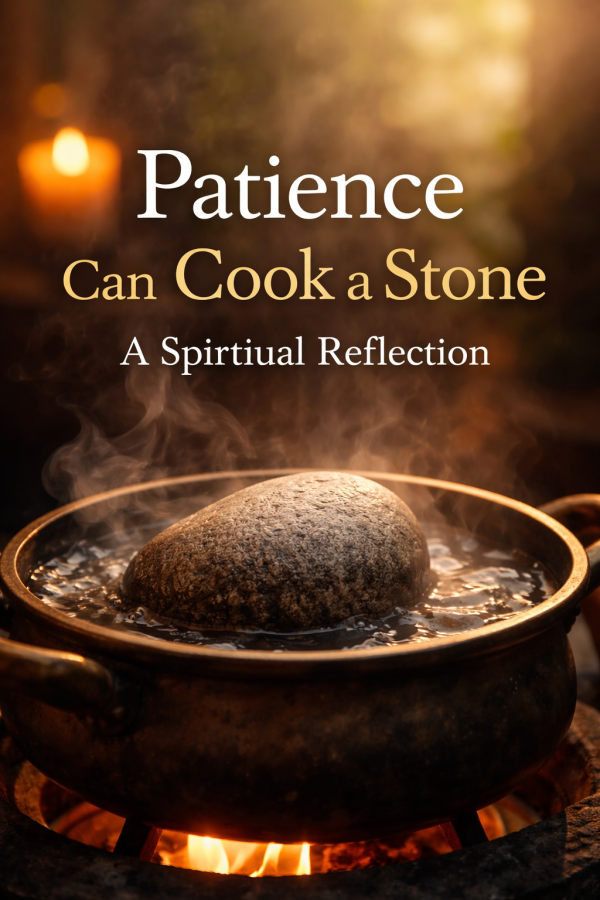रविवार: एक अलसाया पर्व
रविवार आता नहीं, उतरता है —
धीरे-धीरे, नींद की सलवटों में से झाँकता हुआ
जैसे शिशिर की कोई उदास धूप
पुरानी खिड़की से उतर आए चौखट पर।
न यह दिन है, न तिथि —
यह एक विराम है समय की थकी साँसों का,
एक ठहराव — जहाँ जीवन
अपने ही पदचिह्नों को देख मुस्कुरा लेता है।
दुपहरें इस दिन कुछ और होती हैं —
चाय का कप नहीं, स्मृतियों की कटोरी बन जाती हैं,
और रसोई से आती महक
किसी बिसरी हुई बचपन की गली का रास्ता बता देती है।
पिता की ख़ामोशी भी संवाद करती है रविवार को,
माँ की थकान एक दिन की मोहलत पाती है,
और बच्चे —
वे दिनभर आकाश को कैनवस समझते हैं,
बिना किसी पाठ्यक्रम की जेल के।
यह दिन कवियों का भी प्रिय है —
क्योंकि इसमें शब्द नहीं ढूँढने पड़ते,
वे ख़ुद चलकर आ जाते हैं
हाथों में नीम के पत्तों की तरह हरे, कसैले, और सच्चे।
रविवार —
नव-जीवन की एक धीमी चिट्ठी है
जो हर सप्ताह हमारे द्वार पर चुपचाप रख दी जाती है
बिना दस्तक दिए।
-गौतम झा